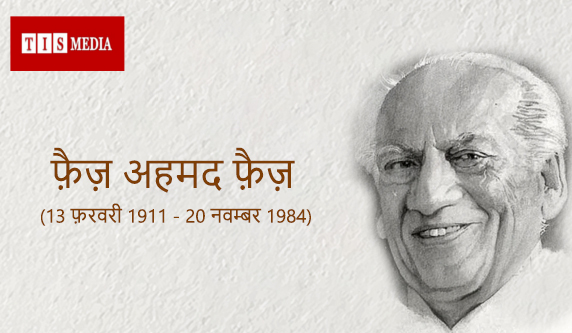निसार मैं तेरी गलियों पे ए वतन, कि जहां चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले…
फैज अहमद फैज की चुनिंदा पांच नज्में, दौर भले ही बदला लेकिन असर नहीं...


फैज़ की नज्में ‘प्रतिरोध’ और ‘साझे प्रयास’ की जरूरतों को समझाती है, जिससे खास तबका परेशान रहता है। इस परेशानी के पीछे 1936 में पहली बार गठित ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के साथ फैज़ का जुड़ाव है। यह संस्था कैसे वजूद में आई, इसका किस्सा दिलचस्प है। बीसवीं शताब्दी में लघु कहानियों की पतली की पुस्तिका ’अंगारे’ ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में हलचल पैदा कर दी। देखते ही देखते राजनीतिक-साहित्यिक आंदोलन की सरगर्मी पैदा हो गई। जब पहली बार लखनऊ में 1932 में दस कहानियों वाली इस पुस्तिका का प्रकाशन हुआ तो हंगामा मच गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत के प्रमुख मुस्लिम मौलवियों और दकियानूसी संगठनों के दबाव में प्रतिबंध लगा दिया। तब केवल कुछ ही प्रतियां छपी थीं। लगभग सभी प्रतियां नष्ट कर दी गईं।
‘नुक्कड़ ए वफा’ में फैज़ ने खुद को ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन के साथ अपने सहयोग पर कहा है: ”अमृतसर में मैं अपने दोस्तों साहिबज़ादा महमूदुज्ज़फ़र और उनकी पत्नी राशिद जहां से मिला। फिर प्रगतिशील लेखक संघ का जन्म हुआ, मजदूरों के आंदोलन शुरू हुए और ऐसा लगा जैसे अनुभव के नए बगीचे (दबिस्तान ) मिल गए हों। इस दौरान मैंने जो पहला पाठ सीखा, वह यह था कि इतनी बड़ी कायनात में खुद के वजूद की पहचान कराने भर की कोशिश महत्वहीन है।”
फैज़ इस नज़रिए से कभी नहीं हटे। उनकी नज्मों में जिंदगी पर दुनिया की घटनाओं और हालात का प्रतिबिंब साफ नजर आता है।
वह कहते हैं, आप किसी के दिमाग में एक मिनट का बदलाव भी लाते हैं … तो आपने व्यवस्था के बदलाव में अपनी भूमिका निभाई होती है। कविता इस काम को काफी हद तक कर सकती है … कविता के लिए नारेबाजी, चिल्लाने और राजनीतिक बयानों जैसी सूरत नहीं होती। ”
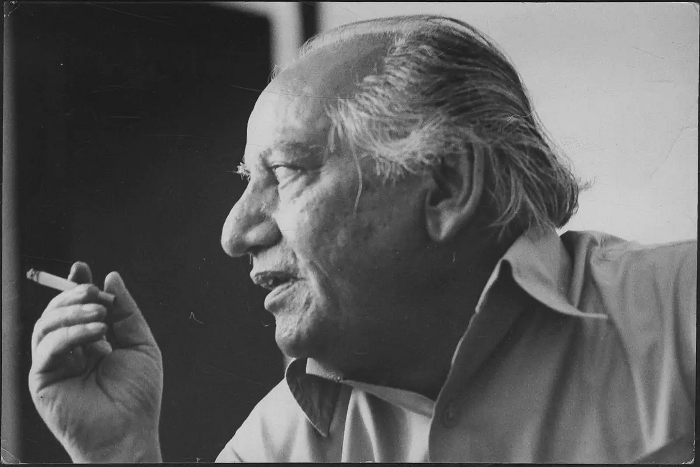
(1)
निसार मैं तेरी गलियों पे ए वतन, कि जहां
चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले
जो कोई चाहनेवाला तवाफ़ को निकले
नज़र चुरा के चले, जिस्म-ओ-जाँ बचा के चले
है अहल-ए-दिल के लिये अब ये नज़्म-ए-बस्त-ओ-कुशाद
कि संग-ओ-ख़िश्त मुक़य्यद हैं और सग आज़ाद
बहोत हैं ज़ुल्म के दस्त-ए-बहाना-जू के लिये
जो चंद अहल-ए-जुनूँ तेरे नाम लेवा हैं
बने हैं अहल-ए-हवस मुद्दई भी, मुंसिफ़ भी
किसे वकील करें, किस से मुंसिफ़ी चाहें
मगर गुज़रनेवालों के दिन गुज़रते हैं
तेरे फ़िराक़ में यूँ सुबह-ओ-शाम करते हैं
बुझा जो रौज़न-ए-ज़िंदाँ तो दिल ये समझा है
कि तेरी मांग सितारों से भर गई होगी
चमक उठे हैं सलासिल तो हमने जाना है
कि अब सहर तेरे रुख़ पर बिखर गई होगी
ग़रज़ तसव्वुर-ए-शाम-ओ-सहर में जीते हैं
गिरफ़्त-ए-साया-ए-दिवार-ओ-दर में जीते हैं
यूँ ही हमेशा उलझती रही है ज़ुल्म से ख़ल्क़
न उनकी रस्म नई है, न अपनी रीत नई
यूँ ही हमेशा खिलाये हैं हमने आग में फूल
न उनकी हार नई है न अपनी जीत नई
इसी सबब से फ़लक का गिला नहीं करते
तेरे फ़िराक़ में हम दिल बुरा नहीं करते
ग़र आज तुझसे जुदा हैं तो कल बहम होंगे
ये रात भर की जुदाई तो कोई बात नहीं
ग़र आज औज पे है ताल-ए-रक़ीब तो क्या
ये चार दिन की ख़ुदाई तो कोई बात नहीं
जो तुझसे अह्द-ए-वफ़ा उस्तवार रखते हैं
इलाज-ए-गर्दिश-ए-लैल-ओ-निहार रखते हैं
(2)
क्यूँ मेरा दिल शाद नहीं है क्यूँ ख़ामोश रहा करता हूँ
छोड़ो मेरी राम कहानी मैं जैसा भी हूँ अच्छा हूँ
मेरा दिल ग़मग़ीँ है तो क्या ग़मग़ीं ये दुनिया है सारी
ये दुख तेरा है न मेरा हम सब की जागीर है प्यारी
तू गर मेरी भी हो जाये दुनिया के ग़म यूँ ही रहेंगे
पाप के फंदे, ज़ुल्म के बंधन अपने कहे से कट न सकेंगे
ग़म हर हालत में मोहलिक है अपना हो या और किसी का
रोना धोना, जी को जलाना यूँ भी हमारा, यूँ भी हमारा
क्यूँ न जहाँ का ग़म अपना लें बाद में सब तदबीरें सोचें
बाद में सुख के सपने देखें सप्नों की ताबीरें सोचें
बे-फ़िक्रे धन दौलत वाले ये आख़िर क्यूँ ख़ुश रहते हैं
इनका सुख आपस में बाँतें ये भी आख़िर हम जैसे हैं
हम ने माना जंग कड़ी है सर फूटेंगे, ख़ून बहेगा
ख़ून में ग़म भी बह जायेंगे हम न रहें, ग़म भी न रहेगा

(3)
हम देखेंगे
लाज़िम है कि हम भी देखेंगे
वो दिन कि जिसका वादा है
जो लोह-ए-अज़ल में लिखा है
जब ज़ुल्म-ओ-सितम के कोह-ए-गरां
रुई की तरह उड़ जाएँगे
हम महकूमों के पाँव तले
ये धरती धड़-धड़ धड़केगी
और अहल-ए-हकम के सर ऊपर
जब बिजली कड़-कड़ कड़केगी
जब अर्ज-ए-ख़ुदा के काबे से
सब बुत उठवाए जाएँगे
हम अहल-ए-सफ़ा, मरदूद-ए-हरम
मसनद पे बिठाए जाएँगे
सब ताज उछाले जाएँगे
सब तख़्त गिराए जाएँगे
बस नाम रहेगा अल्लाह का
जो ग़ायब भी है हाज़िर भी
जो मंज़र भी है नाज़िर भी
उट्ठेगा अन-अल-हक़ का नारा
जो मैं भी हूँ और तुम भी हो
और राज़ करेगी खुल्क-ए-ख़ुदा
जो मैं भी हूँ और तुम भी हो
(4)
हम क्या करते किस रह चलते
हर राह में कांटे बिखरे थे
उन रिश्तों के जो छूट गए
उन सदियों के यारानो के
जो इक –इक करके टूट गए
जिस राह चले जिस सिम्त गए
यूँ पाँव लहूलुहान हुए
सब देखने वाले कहते थे
ये कैसी रीत रचाई है
ये मेहँदी क्यूँ लगवाई है
वो: कहते थे, क्यूँ कहत-ए-वफा
का नाहक़ चर्चा करते हो
पाँवों से लहू को धो डालो
ये रातें जब अट जाएँगी
सौ रास्ते इन से फूटेंगे
तुम दिल को संभालो जिसमें अभी
सौ तरह के नश्तर टूटेंगे ।
(5)
आइए हाथ उठाएँ हम भी
हम जिन्हें रस्मे-दुआ याद नहीं
हम जिन्हें सोज़े-मुहब्बत के सिवा
कोई बुत, कोई ख़ुदा याद नहीं
आइए अर्ज़ गुज़ारें कि निगारे-हस्ती
ज़हरे-इमरोज़ में शीरीनी-ए-फ़र्दां भर दे
वो जिन्हें ताबे गराँबारी-ए-अय्याम नहीं
उनकी पलकों पे शबो-रोज़ को हल्का कर दे
जिनकी आँखों को रुख़े-सुब्हे का यारा भी नहीं
उनकी रातों में कोई शम्म’अ मुनव्वर कर दे
जिनके क़दमों को किसी रह का सहारा भी नहीं
उनकी नज़रों पे कोई राह उजागर कर दे
जिनका दीं पैरवी-ए-कज़्बो-रिया है उनको
हिम्मते-कुफ़्र मिले, ज़ुर्रते-तहक़ीक़ मिले
जिनके सर मुंतज़िरे-तेग़े-जफ़ा हैं उनको
दस्ते-क़ातिल को झटक देने की तौफ़ीक़ मिले
इश्क़ का सर्रे-निहाँ जान-तपाँ है जिससे
आज इक़रार करें और तपिश मिट जाए
हर्फ़े-हक़ दिल में खटकता है जो काँटे की तरह
आज इज़हार करें और ख़लिश मिट जाए…!!!