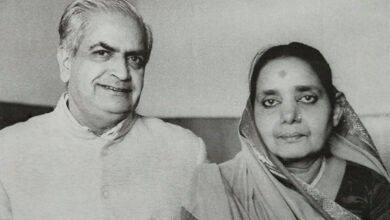कोरोना का कहर: सोशल मीडिया का ज्ञान नहीं, इस जमीनी हकीकत से हों वाकिफ…
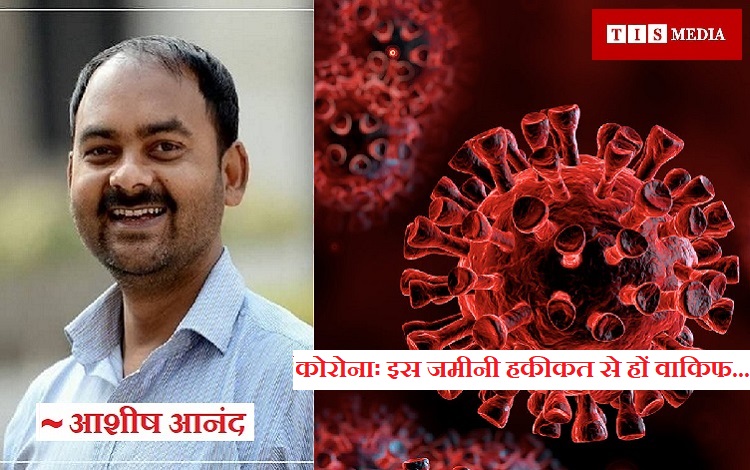
डब्ल्यूएचओ और सीडीसी ने यूके वैरिएंट, ब्राजीलियन वैरिएंट और साउथ अफ्रीकन वैरिएंट के साथ ही अन्य दो को लेकर चिंता जताई है। पहले से पहचाने गए वैरएंट के अलावा भारत में सार्स कोराेना वायरस-2 का डबल म्यूटेंट भी पाया गया है। इसने मौजूद वैक्सीन को लेकर भी चिंता पैदा कर दी है। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में भारत के 18 राज्यों से 10,787 नमूनों के जीनोम के आंकड़े जारी किए हैं, जिनमें ज्ञात वैरिएंट के 771 मामले (7.1%) दिखाए गए हैं। इनमें से 736 यूके वैरिएंट (95.4%) थे, 34 दक्षिण अफ्रीकी वैरिएंट (4.4%) थे और एक ब्राजीलियाई वेरिएंट था। महाराष्ट्र में एक डबल म्यूटेंट का पता चला है।
बेहद अक्रामक है कोरोना का नया वायरस
चिंताजनक रिपोर्ट यह भी है कि टीकाकरण की दूसरी खुराक के 14 दिनों के बाद कम गंभीर रोग से लोग संक्रमित हो जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक mRNA के टीके (Pfizer और Moderna) P1 ब्राजीलियाई वैरिएंट और दक्षिण अफ़्रीकी B.1.351 पर काफी कम प्रभावी हैं। एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन का भी दक्षिण अफ्रीकी कम असर है। हालांकि, यूके वैरिएंट के खिलाफ काफी हद तक कारगर दिखाई दिए हैं। टीकाकरण के अपने जोखिम हैं और वायरस के प्रसार का खतरा भी बरकरार है। डबल म्यूटेंट वाले खोजे गए नए कोरोना वायरस बेहद संक्रामक हैं और इसमें सामान्य संक्रमण या टीकाकरण से पैदा हुई प्रतिरक्षा को नकारने की क्षमता है। यही वजह है कि टीकाकरण वाले लोगों में दोबारा संक्रमण के मामले दुर्लभ नहीं हैं, बहुत से केस हैं। खासतौर पर युवा आबादी इस प्रसार के लिए सुपर स्प्रेडर हैं, जिससे जोखिम कम नहीं है। भारत में तो आबादी भी खासी युवा है। यह जानना भी जरूरी है कि पिछले साल के मुकाबले अभी की स्थिति में क्या खास फर्क है।
यह भी पढ़ेंः कोरोना से इतने खौफजदा क्यों हैं, सच्चाई के इस पहलू से भी वाकिफ होना चाहिए…
COVID की मौजूदा लहर: इस बार क्या बदलाव आया है?
उम्र के रुझान में बदलाव: इस बार गंभीर संक्रामक रोगिायों में कम उम्र या युवा भी बड़ी संख्या में चपेट में आए हैं। वे न केवल संक्रमण से प्रभावित हुए हैं, बल्कि उन्हें आईसीयू में भर्ती करने की भी जरूरत पेश आई है।
आरटी पीसीआर टैस्ट: आरटी पीसीआर परीक्षण COVID मामलों का कुशलता से पता नहीं लगा सकते हैं।
थ्रोंबोटिक विकार: थ्रोम्बोटिक विकार 2020 मामलों के मुकाबले आम हो रहे हैं। रक्त प्रवाह में बाधाएं या थक्का जमने जैसी घटनाएं हो सकती हैं।
टीके: दो खुराक के बावजूद संक्रमण न होने की या प्रतिरोधी होने की गारंटी नहीं है। ऐसे तमाम मरीजों को कोविड लक्षणों के आधार पर अस्पताल लाया गया है। हालांकि, अधिकांश मामलों में आरटी पीसीआर पर कम वायरल लोड और ट्रांसमिशन क्षमता का संकेत मिला है।
उच्च सामाजिक वर्ग पर खतरा: सामाजिक और आर्थिक तौर पर उच्च वर्ग निचले तबके के मुकाबले कहीं ज्यादा पीड़ित है।
विपत्ति: आईसीयू में मरीजों की भर्ती होने वाली मौतें इस बात की गवाह हैं कि संकट किस स्तर पर है, हालांकि इसकी गिरावट जल्द होने की उम्मीद की जानी चाहिए।
रेडियोलॉजिस्ट सीटी घावों से चिंतित हैं: चिंता की बात यह है कि सीटी घावों वाले मामलों का प्रतिशत इस बार बहुत ज्यादा है। कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी से पता चला है कि ब्रेन में सामान्य स्थिति नहीं है, कहीं काले तो कहीं सफेद धब्बे हैं, जो संक्रमण की जद में आने वालों के लिए गंभीर स्थिति है।
यह भी पढ़ें: कोरोना 2.0 पत्रकारों और उनके परिवारों पर भारी पड़ रही ये महामारी
नई लहर अलग कैसे है?
2020 में यह अनुमान लगाया गया था कि SARS-CoV सर्द मौसम की घटना है, हालांकि 2021 में वायरस ने सभी को गलत साबित कर दिया, इटली जैसा सर्द मौसम होना तो नहीं ही साबित हुआ। किसी सतह के जरिए वायरस का प्रसार होना अब अहम चिंता का विषय नहीं है। अब एयर ट्रांसमिशन की परिकल्पना पर जोर है।
क्या आरटी-पीसीआर अभी भी इन स्थितियों में लागू है?
RT PCR परीक्षण COVID-19 को ट्रिगर करने वाले सभी वैरिएंट का पता लगा सकता है, लेकिन कुछ नए म्यूटेंट इससे ट्रेस नहीं भी हो सकते हैं। इस वजह से चिकित्सकों के सामने डायग्नोसिस को लेकर संदेह बढ़ा है। सीरम मार्कर और सीटी का इस्तेमाल जरूरी है गंभीरता मापने को। बीमारी की पहचान के पहले दिन जब रोगी अस्वस्थ महसूस करना शुरू कर देता है, इस समय कोविड प्रबंधन प्रक्रिया सबसे अहम होती है, समय का उपयोग सबसे जरूरी है। लक्षण उभरने के एक दिन पहले और तीन से चार दिन बाद वायरस अधिक संक्रामक होता है। रोगी को पहले 2-3 दिनों तक तेज बुखार होने की आशंका होती है, लेकिन इस स्तर पर मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल और अन्य कोशिकाएं जन्मजात प्रतिरक्षा वायरस के खिलाफ प्रतिक्रिया देना शुरू कर देती है। अतिरिक्त ऑक्सीजन की जरूरत, हाइपोक्सिया और अन्य लक्षण दूसरे सप्ताह में शुरू होते हैं। ऐसे में 7 से 10 दिनों के भीतर निरोधक दवाओं से नियंत्रण करने की कोशिश जरूरी होती है। सही समय पर कई आधुनिक दवाएं, जैसे कि स्टेरॉयड, टोसीलिज़ुमाब और प्लाज्मा, अच्छी तरह से काम करती हैं।
यह भी पढ़ें: चिट्ठी में छलका डॉक्टर का दर्द, बोलेः कितने भी संसाधन हम जुटा लें, इस महामारी में कम पड़ेंगे
इस तरह होती है संक्रमण की पहचान और इलाज की शुरुआत
– वायरस के संपर्क में आने के बाद दो दिन से लेकर दो सप्ताह तक संक्रमण के लक्षण दिखाई देने लगते हैं
– संक्रमण 15 मिनट में हो सकता है
– रोग आमतौर पर 4 से 5 दिनों के बीच होने दिखने का अनुमान है
– वायरस 9 दिनों के बाद खुद को दोहराता नहीं है
– संक्रमण के संदेह पर तीसरे से छठे दिन के बीच छह मिनट की वॉक टेस्ट मददगार साबित हो सकता है।
बुखार 101 डिग्री फारेनहाइट, CRP में तेज बढ़ोत्तरी होती है जो लीवर द्वारा बनने वाला प्रोटीन होता है, इसके बढ़ने का मतलब संक्रमण होता है, इसके अलावा 3 दिन में खांसी या छह मिनट की वॉक टेस्ट में SpO2 में 5 प्रतिशत की गिरावट, निमोनिया चेतावनी के संकेत हैं। लैंसेट 2020 फी Z एट अल की रिपोर्ट के अनुसार कोविड संक्रमण का पांचवां दिन सबसे गंभीर समय होता है।
(15 सालों से पत्रकारिता के खांटी हस्ताक्षर आशीष आनंद दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे अखबारों से जुड़े रहे हैं। फिलहाल वह स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं एवं TIS Media की उत्तर प्रदेश टीम का प्रमुख हिस्सा हैं।)